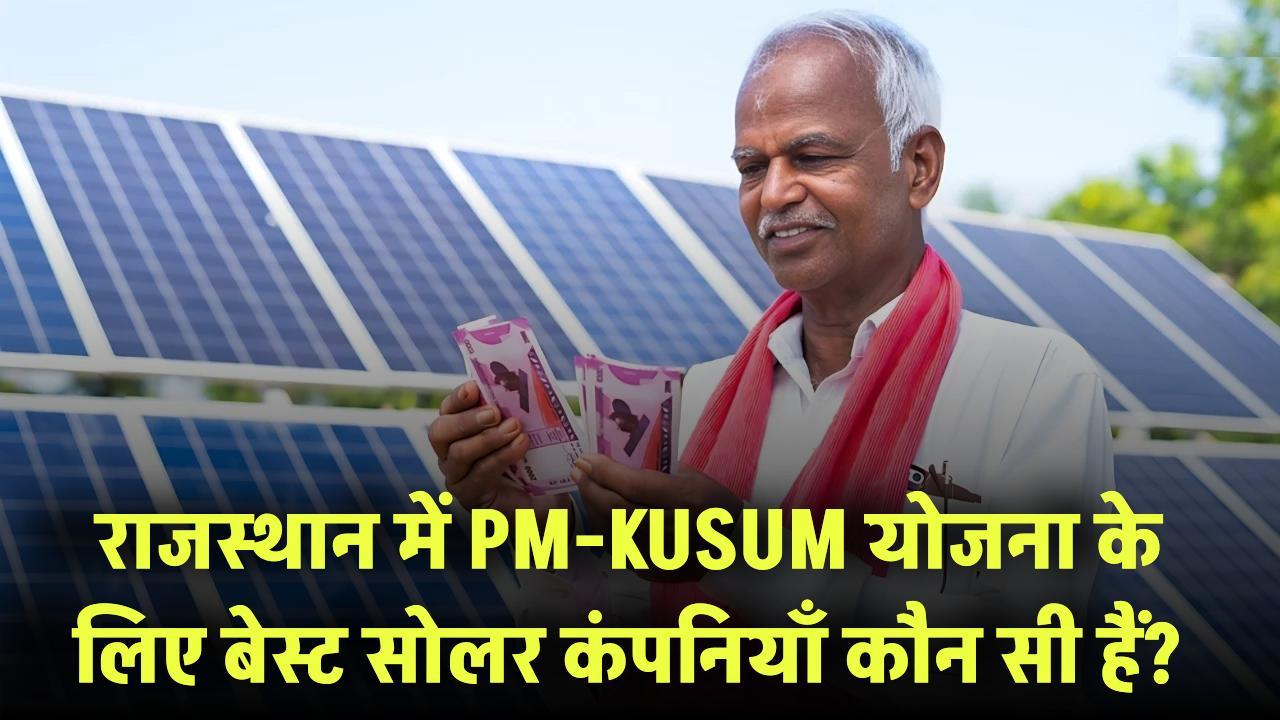भारत में तेजी से बढ़ती ऊर्जा जरूरतों और रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy की मांग के बीच हाइड्रोजन सोलर पैनल-Hydrogen Solar Panel तकनीक को भविष्य के सबसे स्वच्छ और आत्मनिर्भर बिजली समाधान के रूप में देखा जा रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि इस तकनीक की मदद से 24 घंटे बिना किसी बिजली कटौती के पावर सप्लाई मिल सकती है, और वह भी पूरी तरह ग्रीन एनर्जी से। लेकिन क्या यह विकल्प आम भारतीय घरों के लिए वाकई में व्यावहारिक और किफायती साबित हो सकता है? इस रिपोर्ट में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढ़ने की कोशिश करेंगे।
हाइड्रोजन सोलर पैनल सिस्टम कैसे करता है काम?
हाइड्रोजन पर आधारित यह तकनीक तीन मुख्य भागों पर निर्भर करती है—इलेक्ट्रोलाइज़र, हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक और फ्यूल सेल। सबसे पहले, इलेक्ट्रोलाइज़र सौर पैनलों से मिलने वाली बिजली का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करता है। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। इसके बाद जो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है, उसे विशेष टैंकों में संग्रहित किया जाता है।
जब सूरज उपलब्ध नहीं होता, जैसे कि रात में या मानसून के मौसम में, तब स्टोरेज में रखे गए हाइड्रोजन को फ्यूल सेल के ज़रिए पुनः बिजली में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में केवल जल-वास्प निकलता है, जिससे यह एक बेहद स्वच्छ ऊर्जा स्रोत बन जाता है। कनाडा में इस तकनीक पर आधारित एक प्रोटोटाइप सिस्टम ने 24×7 बिजली सप्लाई का सफल परीक्षण भी किया है।
भारत में लागत कितनी है और क्या यह आम आदमी के बजट में है?
भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की वर्तमान लागत ₹350 से ₹450 प्रति किलोग्राम तक है, जो कि ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में बहुत अधिक है। ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से तैयार की जाती है और यह लागत में अपेक्षाकृत सस्ती होती है। हालांकि, सरकार की योजनाएं और तकनीकी प्रगति इस अंतर को कम करने की दिशा में काम कर रही हैं।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत ₹260 से ₹310 प्रति किलोग्राम तक आ सकती है। लेकिन यदि बात की जाए एक पूर्ण घरेलू हाइड्रोजन सिस्टम की, तो इसकी स्थापना लागत अभी ₹10 लाख से ₹20 लाख के बीच आंकी जाती है। इसमें इलेक्ट्रोलाइज़र, स्टोरेज टैंक और फ्यूल सेल जैसी जटिल और महंगी तकनीकों का इस्तेमाल होता है। इस वजह से यह सिस्टम अभी आम भारतीय परिवारों की पहुंच से बाहर है।
सरकार की नीतियां और हाइड्रोजन तकनीक का भविष्य
भारत सरकार ने National Green Hydrogen Mission के तहत 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए लगभग ₹17,000 करोड़ (यानी $2.1 बिलियन) का निवेश प्रस्तावित किया गया है। यह मिशन भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
यह भी पढ़े-भारत में 1kW सोलर पैनल की कीमत कितनी है? जानें इंस्टॉलेशन से लेकर सब्सिडी तक की पूरी डिटेल
सरकार की इस पहल से न केवल घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि हाइड्रोजन तकनीक के क्षेत्र में नवाचार और प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलेगा। टेलीकॉम टावरों, रेलवे और भारी उद्योगों में इस तकनीक का परीक्षण और उपयोग पहले से शुरू हो चुका है। आने वाले वर्षों में इसके लागत में गिरावट और उत्पादन में वृद्धि संभावित है, जिससे यह घरेलू उपयोग के लिए भी एक व्यवहारिक विकल्प बन सकता है।
मौजूदा समय में क्या विकल्प बेहतर हैं?
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो सोलर पैनल और बैटरी स्टोरेज का संयोजन आम उपभोक्ताओं के लिए एक अधिक व्यावहारिक और सस्ता विकल्प है। इन प्रणालियों की लागत ₹1.5 लाख से ₹3 लाख के बीच होती है और इनमें रख-रखाव भी अपेक्षाकृत कम होता है। साथ ही, कई राज्य सरकारें इस पर सब्सिडी भी प्रदान कर रही हैं जिससे यह और भी सुलभ बनता जा रहा है।
जहां हाइड्रोजन सिस्टम तकनीकी रूप से भविष्य के लिए बेहतर हो सकता है, वहीं मौजूदा समय में इसके मुकाबले सोलर-बैटरी समाधान ज़्यादा सटीक और स्थापित हैं। छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह एक व्यवहारिक और भरोसेमंद समाधान बना हुआ है।
हाइड्रोजन तकनीक का सफर अभी बाकी है
हाइड्रोजन सोलर पैनल-Hydrogen Solar Panel तकनीक एक क्रांतिकारी सोच है जो भारत को 100% Self Dependent बिजली की दिशा में ले जा सकती है। यह न केवल स्वच्छ है, बल्कि लॉन्ग टर्म में टिकाऊ भी है। हालांकि, इस वक्त इसकी लागत और तकनीकी सीमाओं के चलते यह आम घरों के लिए एक कठिन विकल्प बना हुआ है।
सरकार की योजनाओं, स्टार्टअप्स की भागीदारी और तकनीकी नवाचार के साथ आने वाले वर्षों में इस तकनीक की लागत में गिरावट आ सकती है। लेकिन जब तक यह व्यवहारिक रूप से किफायती और सरल नहीं होती, तब तक सोलर पैनल-बैटरी संयोजन ही घरेलू बिजली जरूरतों का सबसे अच्छा विकल्प बना रहेगा।